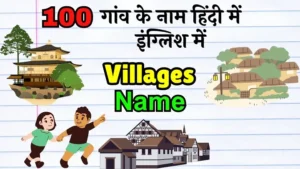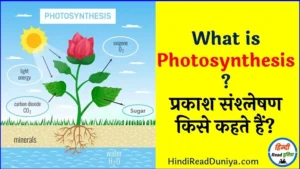रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार, रस की परिभाषा, उदाहरण Ras ki Paribhasha udaharan sahit, ras kise kahate hain class 10
Table of Contents
रस किसे कहते हैं? Ras kise kahate hain?
कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनन्द की अनुभूति होती है, उसे ‘रस‘ कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना गया है।
भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति के संबंध में लिखा है – विभावानुभावव्यभिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्तिः जिसका अर्थ है (1) स्थायी भाव, (2) विभाव, (3) अनुभव, (4) संचारी भाव (व्यभिचारी भाव) के सहयोग से रस निष्पत्ति होती है।
रस के स्थायी भाव के प्रकार
रस रूप में पुष्ट या परिणत होनेवाला तथा सम्पूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहनेवाला भाव स्थायी भाव कहलाता है। स्थायी भाव नौ माने गये हैं—रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। वात्सल्य-प्रेम नाम का दसवाँ स्थायी भाव भी स्वीकार किया जाता है।
रति – स्त्री-पुरुष के परस्पर प्रेम-भाव को रति कहते हैं।
हास – किसी के अंगों, वेश-भूषा, वाणी आदि के विकारों के ज्ञान से उत्पन्न प्रफुल्लता को हास कहते हैं।
शोक – इष्ट के नाश अथवा अनिष्टागम के कारण मन में उत्पन्न व्याकुलता शोक है।
क्रोध – अपना काम बिगाड़नेवाले अपराधी को दण्ड देने के लिए उत्तेजित करनेवाली मनोवृत्ति क्रोध कहलाती है।
उत्साह – दान, दया और वीरता आदि के प्रसंग से उत्तरोत्तर उन्नत होनेवाली मनोवृत्ति को उत्साह कहते हैं।
भय – प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देखकर मन में जो व्याकुलता होती है, उसे भय कहते हैं।
जुगुप्सा – घृणा उत्पन्न करनेवाली वस्तुओं को देखकर उनसे सम्बन्ध न रखने के लिए बाध्य करनेवाली मनोवृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं।
विस्मय – किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर जो आश्चर्य होता है, उसे विस्मय कहते हैं।
निर्वेद – संसार के प्रति त्याग-भाव को निर्वेद कहते हैं।
वात्सल्य – पुत्रादि के प्रति सहज स्नेह-भाव वात्सल्य है।
विभाव किसे कहते हैं?
उत्तेजना के मूल कारण को विभाव कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं – आलम्बन और उद्दीपन।
आलम्बन विभाव किसे कहते हैं? जिसके कारण से आश्रय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आलम्बन कहा जाता है। जैसे – जंगल में शेर को देखकर जब कोई व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तो यहाँ पर भय का आलम्बन शेर होगा।
उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त या तीव्र होने लगे उस कारण को ही उद्दीपन कहा जाता है। जैसे- कोई व्यक्ति सुनसान अंधेरे जंगल में शेर को देखकर भयभीत हो जाय; तो यहाँ पर सुनसान, अँधेरा जंगल आदि उद्दीन विभाव होंगे। क्योंकि इनके कारण ही भय में वृद्धि हो रही है।
अनुभाव किसे कहते हैं?
किसी व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जाग्रत होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएँ अनुभाव कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे – शेर से डरकर व्यक्ति का काँपने लगना, भागने लगना, बेहोश हो जाना आदि अनुभाव है। अनुभाव के 5 प्रकार माने गए हैं – (1) कायिक, (2) वाचिक, (3) मानसिक, (4) सात्विक, तथा (5) आहार्य
संचारी भाव किसे कहते है और कितने होते हैं?
स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए कुछ समय के लिए जागकर समाप्त होने वाले भाव संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। जैसे- शेर से भयभीत व्यक्ति को यह याद आ जाय कि इस स्थान पर कुछ समय पूर्व शेर ने एक आदमी को मार दिया था। तो इस स्मृति संचारी से उसका भय कई गुना बढ़ जाएगा।
भरत मुनि ने संचीरी भावों की संख्या 33 मानी है जो इस प्रकार है-
| 1. निर्वेद | 18. गर्व |
| 2. ग्लानि | 19. विषाद |
| 3. शंका | 20. औत्सुक्य |
| 4. असूया | 21. निद्रा |
| 5. मद | 22. अपस्मार |
| 6. श्रम | 23. स्वप्न |
| 7. आलस्य | 24. विबोध |
| 8. दैन्य | 25. अमर्ष |
| 9. चिंता | 26. अविहित्था |
| 10. मोह | 27. उग्रता |
| 11. स्मृति | 28. मति |
| 12. घृति | 29. व्याधि |
| 13. ब्रीडा | 30. उन्माद |
| 14. चपलता | 31. मरण |
| 15. हर्ष | 32. वितर्क |
| 16. आवेग | 33. भय |
| 17. जड़ता |
रस के प्रकार और स्थायी भाव
| क्र. | रस के प्रकार | रस के स्थायी भाव |
|---|---|---|
| 1. | श्रृंगार रस | रति |
| 2. | हास्य रस | हास |
| 3. | करुण रस | शोक |
| 4. | रौद्र रस | क्रोध |
| 5. | वीर रस | उत्साह |
| 6. | भयानक रस | भय |
| 7. | वीभत्स रस | जुगुप्सा, घृणा |
| 8. | अद्भुत रस | विस्मय |
| 9. | शान्त रस | निर्वेद, वैराग्य |
| 10. | वत्सल रस | वात्सल्य-प्रेम |
यह भी पढ़े
- 250 हिंदी मुहावरे और उनके अर्थ और वाक्यों में प्रयोग उदाहरण सहित
- 100 लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ
- आसमान नीला क्यों दिखाई देता है?
श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित
जब सहृदय के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तो वह शृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इसके दो भेद होते हैं- संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार या विप्रलम्भ
1. संयोग श्रृंगार – नायक और नायिका के मिलन का वर्णन संयोग शृंगार कहलाता है।
स्थायी भाव – रति। आलम्बन – नायक या नायिका। उद्दीपन – नायक या नायिका का मोहक रूप, एकान्त, नदी का किनारा, चाँदनी रात, फुलवारी आदि। अनुभाव – अपलक निहारना, रोमांच दर्शन, स्पर्श, स्वर-भंग, हास्य कटाक्ष, संकेत, मुस्काना आदि। संचारी भाव – हर्ष, संकोच आदि।
संयोग श्रृंगार उदाहरण –
राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाहीं।
यातें सबै सुधि भूलि गयी, कर टेकि रही पल टारत नाहीं।
स्पष्टीकरण–
स्थायी भाव – रति
आश्रय – सीता
आलम्बन – राम
उद्दीपन – राम का रूप
अनुभाव – रूप निहारना, सुधि भूल जाना।
संचारी भाव – सुधि भूलना।
2. वियोग श्रृंगार – जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह वर्णन होता है, वहाँ वियोग शृंगार होता है।
वियोग शृंगार के उदाहरण-
मेरे प्यारे जलद से कंज से नेत्रवाले।
जाके आये न मधुबन से औ न भेजा संदेशा।
मैं रो रो के प्रिय-विरह से बावली हो रही हूँ।
जा के मेरी सब दुख-कथा श्याम को तू सुना दे॥
स्पष्टीकरण–
स्थायी भाव – रति
आश्रय – राधा
आलम्बन – श्रीकृष्ण
उद्दीपन – शीतल, मन्द पवन और एकान्त
अनुभाव – रूप निहारना, सुधि भूल जाना।
संचारी भाव – स्मृति, रुदन, चपलता, आवेग, उन्माद
करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित
सहृदय के हृदय में शोक नामक स्थित भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भीव के साथ संयोग होता है तो वह करुण रस का रूप ग्रहण कर लेता है।
करुण रस के उदाहरण –
जा थल कीन्हैं बिहार अनेकन ता थल काँकरि चुन्यौ करै।
जा रसना ते करी बहुबातन ता रसना ते चरित्र गुन्यों करै।
‘आलम’ जौन से कुंजन में करि केलि तहाँ अब सीस धुन्यों करै।
नैनन में जो सदा रहते तिनकी, अब कान कहानी सुन्यों करै।
स्पष्टीकरण–
स्थायी भाव – शोक
आश्रय – प्रियतमा
आलम्बन – प्रिय मरण
उद्दीपन – दयनीय दशा, करुण विलाप।
अनुभाव – अश्रु, निःश्वास, प्रलाप
संचारी भाव – स्मृति, दैन्य, आवेश, विषाद।
उदाहरण 2 –
देखि सुदामा की दीन दसा, करुणा करिके करुणानिधि रोए।
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैननि के जल सों पग धोए।।
हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित
जब सहृदय के हृदय में स्थित हास्य नामक स्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भीव के साथ संयोग होता है तो वह हास्य रस कहलाता है।
हास्य रस का उदाहरण –
इस दौड़-धूप में क्या रखा आराम करो, आराम करो।
आराम जिन्दगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है।
आराम सुधा की एक बूँद, तन का दुबलापन खोती है।
आराम शब्द में राम छिपा, जो भव-बंधन को खोता है।
आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है।
इसलिए तुम्हें समझाता हूँ मेरे अनुभव से काम करो।
स्पष्टीकरण–
स्थायी भाव – हास
आश्रय –
आलम्बन – हास्य पात्र
उद्दीपन – व्यंगोक्ति
अनुभाव – खिलखिलाना
संचारी भाव – हर्ष, चपलता, निर्लज्जता।
वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित
जब सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भीव के साथ संयोग होता है तो वह वीर रस का रूप ग्रहण कर लेता है। ‘वीर रस’ में वीरता, बलिदान, राष्ट्रीयता जैसे सद्गुणों का संचार होता है। और दान, दया, धर्म युद्ध एवं वीरता के भाव वीर रस की विशेषताएं होती है।
वीर रस का उदाहरण-
सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भृकुटी तानी थी।
बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झासी वाली रानी थी।
स्पष्टीकरण–
स्थायी भाव – उत्साह
आश्रय – हनुमान
आलम्बन – मेघनाद
उद्दीपन – कटक की विह्वल दशा।
अनुभाव – महान् शैल को उखाड़ना और फेंकना।
संचारी भाव – स्वप्न की चिंता, शत्रु की रिस (क्रोध, अमर्ष) उग्रता और चपलता।
रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित
जब सहृदय का क्रोध नामक स्थाईभाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस का रूप ग्रहण कर लेता है।
रौद्र रस का उदाहरण:
श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे।
सब शोक अपना भूलकर, करतल युगल मलने लगे।।
संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े।
करते हुए यह घोषणा, वे हो गए उठकर खड़े।।
उस काल मारे क्रोध के तन काँपने उनका लगा।
मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।।
स्पष्टीकरण–
स्थायी भाव – क्रोध
आश्रय – अर्जुन
आलम्बन – शत्रु
उद्दीपन – श्रीकृष्ण के वचन
अनुभाव – क्रोध पूर्ण घोषणा
संचारी भाव – आवेग, चपलता, श्रम, उग्रता आदि।
भयानक रस की परिभाषा उदाहरण सहित
भय नामक स्थाई भाव का जब विभाव, अुनभाव, संचारी भाव से संयोग मिलता है, तब भयानक रस का रूप ग्रहण कर लेता है।
भयानक रस का उदाहरण :
नभ से झपटत बाज लखि, भूल्यो सकल प्रपंच।
कंपति तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच।।
स्पष्टीकरण–
स्थायी भाव – भय
आश्रय – लावा पक्षी
आलम्बन – बाज
उद्दीपन – बाज का झपटना
अनुभाव – शरीर का कापना
संचारी भाव – दैन्य विषाद काँपना
अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित
जब विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुवभाव और संचारी भाव से संयुक्त होकर जिस भाव का उद्रेक होता है वह अद्भुत रस ग्रहण कर लेता है।
अद्भुत रस का उदाहरण-
अखिल भुवन चर-अचर सब, हरि मुख में लखि मातु।
चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकातु।।
स्पष्टीकरण–
स्थायी भाव – विस्यम
आश्रय – माता यसोदा
आलम्बन – श्रीकृष्ण का मुख
उद्दीपन – मुख में भुवनों का दिखना
अनुभाव – नेत्र विकास
संचारी भाव – त्रास और जड़ता।
वीभत्स रस की परिभाषा उदाहरण सहित
सहृदय के हृदय मे स्थित जुगुप्सा (घृणा) नामक स्थाई भाव का जब विभाव, अुनाभाव और संचारीभाव का संयोग हो जाता है। तो वह वीभत्स रस का रूप ग्रहण कर लेता है।
वीभत्स रस का उदाहरण-
सिर पर बैठे काग, आंख दोऊ खात निकारत।
खीचति जीभहिं स्यास, अतिहि आनन्द उर धारत।।
बहु चील्ह नोच लै जात मोद बढ़ौ सब कौ हियौ।
मनु ब्रह्मा भोज जिजमान कोऊ आज भिखारिन कहँ दियो।।
स्पष्टीकरण–
स्थायी भाव – जुगुप्सा (घृणा)
आश्रय –
आलम्बन – श्मशान का दृश्य
उद्दीपन – अंतड़ी की माला पहनना, धड़ पर बैठकर कलेजा को फाड़कर निकालना
अनुभाव –
संचारी भाव – निर्वेद ग्लानि
शान्त रस की परिभाषा उदाहरण सहित
संसार की निस्सारता तथा इसकी वस्तुओं की नश्वरता का अनुभव करते हृदय में वैराग्य या निर्वेद भाव उत्पन्न होता है। यही निर्वेद स्थाई भाव, विभाव, अुनभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शांत रस में परिणत होता है।
शान्त रस का उदाहरण-
मन रे ! परस हरि के चरण
सुभग सीतल कमल कोमल,
त्रिविध ज्वाला हरण।
स्पष्टीकरण–
स्थायी भाव – निर्वेद
आश्रय – भक्त हृदय
आलम्बन – अनित्य संसार
उद्दीपन – अनुराग, भोग, विषय, काम
अनुभाव – उन्हें छोड़ देने का कथन
संचारी भाव – धृति, मति, विमर्ष।
वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित
जहाँ सहृदय के मन में वात्सल्य प्रेम नामक स्थाई भाव से जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव मिलते हैं, तब वह वात्सल्य रस का रूप ग्रहण कर लेता है।
वात्सल्य रस का उदाहरण-
जसोदा हरि पालने झुलावै।
हलरावै, दुलराई, मल्हावै, जोइ सोइ कछु गावै।।
मेरे लाल को आउ निंदरिया, काहे न आनि सुलावै।
तू काहे नहिं बेगहिं आवत, ताकौं कान्ह बुलावै।।
कबहूँ पलक हलि मूँद लेत, कबहुँ अधर फरकावै।
सोवत जानि मौन ह्वै कै रहि, करि-करि सैन बतावै।।
स्पष्टीकरण–
स्थायी भाव – वात्सल्य प्रेम
आश्रय – यसोदा
आलम्बन –
उद्दीपन – कृष्ण को सुलाना, पलक मूँदना।
अनुभाव – यशोदा की क्रियाएँ।
संचारी भाव – शंका, हर्ष आदि।
FAQ Ras kise kahate hain
रस कितने प्रकार के होते हैं class 10
Types of Ras – रस के 10 प्रकार होते हैं-
(1) शृंगार रस (2) हास्य रस (3) करुण रस (4) रौद्र रस (5) वीर रस (6) भयानक रस (7) वीभत्स रस (8) अदभुत रस (9) शान्त रस (10) वात्सल्य रस
शृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं?
शृंगार रस दो प्रकार के होते हैं- (1) संयोग श्रृंगार (2) वियोग श्रृंगार
जहां पर नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है।
जहां पर नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो वहां वियोग श्रृंगार होता है।
शान्त रस का स्थायीभाव क्या है?
शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इस रस में तत्व ज्ञान कि प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शान्ति मिलती है उसे शान्त रस कहते हैं।
तो दोस्तों आज हमने आपको रस के सभी भेद के बारे में बताया रस किसे कहते हैं? रस के प्रकार, रस की परिभाषा, उदाहरण के साथ तथा रस से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया है। अगर आपको यह जानकारी ras kise kahate hain अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ share ज़रुर करे। पोस्ट को यहाँ तक पढ़ने के लिए धन्यवाद!
Related Post
- Daily Use English Sentences for Hindi Speakers

- 100 everyday objects Name in Hindi and English

- Private, Government, Bank Me Job Kaise Paye? सरकारी बैंक में नौकरी कैसे मिलेगी

- 100 गांव के नाम हिंदी में और इंग्लिश में | Village Name in Hindi and English

- फोटोसिंथेसिस क्या होता है: जानिए पौधों के जीवनसंचालन की अद्वितीय प्रक्रिया